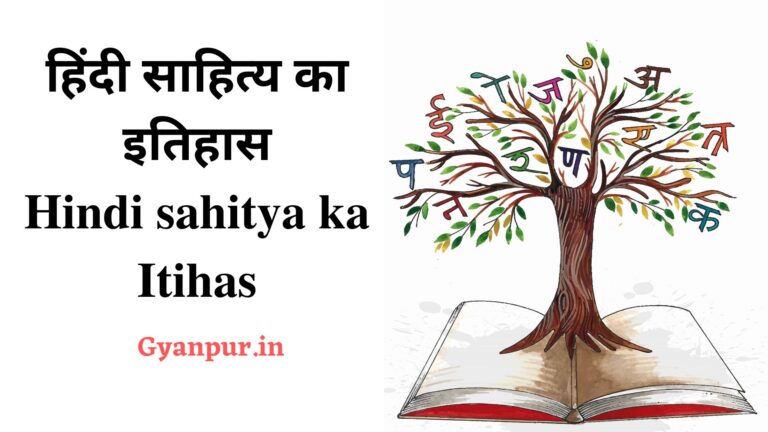हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास 2022-2023 ।
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास अपने आप में ही परिचय का मोहताज नहीं है हिंदी एक ऐसी भाषा जो युगों युगांतर से भारतवर्ष में प्रचलित है ऐसे ही आज हम अध्ययन करने वाले हैं उसी महान हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में के हिंदी पद साहित्य का इतिहास क्या था हिंदी पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा।
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास पर 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं यह प्रश्न बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय प्रकार के हो सकते हैं। यदि आप अपने इन अंको को परीक्षा में सुनिश्चित करना चाहते हैं जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं इसलिए आपको हिंदी पद साहित्य का इतिहास अवश्य देखना चाहिए।
हिंदी पद साहित्य के इतिहास को अनेक कार्यों में विभाजित किया गया है जो कि आपको निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं–
हिंदी पद्य साहित्य का संपूर्ण इतिहास हिंदी में।
हिंदी पद्य साहित्य का संपूर्ण इतिहास हिंदी में जानना अगर आप चाहते है तो हम जानते है आप अपनी परीक्षा की वजह से थोड़ा नर्वस है बिलकुल हम आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास वर्णित मिलेगा। कियोंकि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास संक्षेप में जानने को मिलेगा। पद्य साहित्य किसे कहते हैं एवं पद्य साहित्य की परिभाषा तथा पद्य साहित्य का काल विभाजन सभी जानकारी आपको सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जानें।
आदिकाल (हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास)
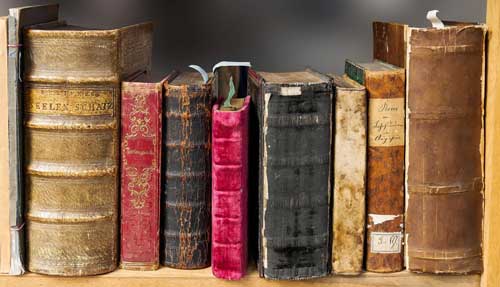
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आदिकाल की समय अवधि हिंदी पद्य के साहित्य में 700 से 1400 ईसवी तक बताई गई है तथा अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है जो 769 ईसवी में अपने अस्तित्व में आए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान जो कि 13वीं सदी में आए थे।
उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है अर्थात हिंदी के प्रथम कवि के बारे में अलग-अलग विद्वानों के अपने-अपने मत हैं अतः स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता के आदिकाल का या हिंदी का प्रथम कवि कौन था। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान करत संदेश रासक जो कि एक खंडकाव्य है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास की दृस्टि से यह काल काफी महत्वपूर्ण था।
| रचना | रचनाकार |
| दोहा कोश | सरहपा |
| चर्या पद | शबरपा |
| डोंबी गीतिका योगचर्या आदि | डोंभिपा |
84 शब्दों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा जो कि सबरपा के शिष्य थे इनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता होती थी। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ को बताया जाता है।
गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने गोरखबानी नाम से किया है इसमें खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है।
जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास को बताया गया है । जैन परंपरा की सर्वप्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है।
चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल आदि भाषाओं को माना जाता है। परमाल रासो को आल्हाखंड भी कहा जाता है। चंपू काव्य एक गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। इसकी प्राचीनतम कृति राउलवेल 10 वीं सदी के अरोड़ा नामक कवि द्वारा रचित की गई। इसी का वैसे हिंदी में नक्शे का वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ हुआ।
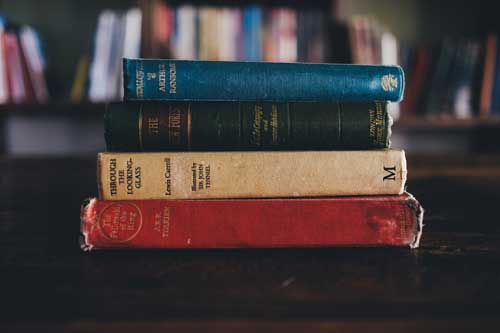
वही खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो एटा के पटियाली गांव से जन में कवि थे।
कुछ श्रृंगार रस के सिद्ध कवियों के नाम निम्नलिखित हैं जैसे मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, गंगा–वाक्यवली, पदावली आदि।
जैन साहित्य में राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ साल भद्र सूर्य किरण भारतेश्वर बाहुबली रास
ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है
हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति साहित्य से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है।
हिंदी में के पदों की परंपरा शब्दों से शुरू हुई थी, मैं दोहा चौपाई की परंपरा सरहपा ने प्रारंभ की थी, ब्रज भूल बंगाल असम में ब्रजभाषा से प्रभावित बांग्ला एवं असमिया भाषा है।
भक्ति काल
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में आदिकाल के बाद भक्ति काल की शुरुआत होती है जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि आदिकाल 700 से 1400 ईसवी तक चला। इसका तात्पर्य है कि भक्ति काल का आरंभ संत 1400 ईस्वी से हुआ, तथा यह 1700 ईस्वी तक चला भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय कहलाया।
भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय बेशरा संप्रदाय के कहलाया। निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद्भागवत को माना जाता है हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कवि नामदेव थे। संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन नाथ पंथ इस्लाम सूफी दर्शन और बौद्ध धर्म को माना जाता है।
पूर्णता अद्वैत वादी कवि कबीर दास को माना जाता है तथा भक्तमाल के रचयिता नाभादास माना जाता है। जायसी पद्मावत की भाषा एकदम से ठेठ अवधी भाषा है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास काफी महत्वपूर्ण विषय है।
| प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत | प्रवर्तक |
| अद्वैतवाद | शंकराचार्य |
| विशिषिष्ठद्वेतवाद | रामानुजाचार्य |
| द्वैतवाद | मध्यवाचार्य |
| द्वैतद्वैतवाद | निंबार्काचार्य |
| शुद्धद्वैतावाद | वल्लभाचार्य |
सूफी शब्द सूफ से निर्मित हुआ था। जिसका अर्थ पवित्र होता है। सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की थी जबकि तुलसीदास की भक्ति दास स्वभाव की थी। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास इन दोनों कवियों अतुल्य योगदान को कभी भुला नहीं पायेगा।
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बताता है कि भक्ति काव्य धारा की दो शाखाएं हैं
निर्गुण काव्यधारा–जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है।
सगुण काव्य धारा–जिसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है।
निर्गुण काव्यधारा
निर्गुण काव्यधारा पुनः ज्ञानश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रय शाखा में विभाजित हो गई। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास निर्गुण काव्यधारा को काफी महत्वपूर्ण काव्यधारा बताता है।
ज्ञानश्रयी शाखा–यह शाखा उपासना ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित काव्य धारा थी। डॉ रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा का नाम दिया है। इस शाखा में जीवन की जटिलताओं से मुक्ति के लिए सहज प्रेम ज्ञान एवं सदाचारी जीवन को आवश्यक बताया है। समाज में व्याप्त आडंबरों अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में प्रेम एवं एकता की स्थापना पर इस शाखा में जोड़ दिया गया है। इस शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर दास को प्रस्तुत किया गया है जो कि रामानंद के शिष्य थे।
इस शाखा के अन्य कवि जैसे रैदास नानक देव दादू दयाल मलूक दास सुंदर दास रज्जाब आदिकवि थे। निर्गुण साहित्य की प्रधान विशेषता रही है कि इसमें गुरुमहिमा, सदाचरण का महत्व, नाम–स्मरण, जप, कीर्तन, प्रेम–प्रकर्ष, अनुभूति का उत्कर्ष, सर्वआत्मा–भाव समर्पण देन्य का भाव आदि। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास इस शाखा के कवियों का सम्मान करता है।
प्रेमाश्रय शाखा–यह शाखा प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखती है भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान सूफी फकीर इश्क मजा जी से इश्क हकीकी तक पहुंचने में विश्वास करते थे। प्रेमाश्रय काव्य की कथावस्तु में लोक कथाओं इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण मिलता है इनकी रचनाएं तथा उनकी शैली मसनवी थी। प्रतिनिधि कवि के रूप में जायसी के अतिरिक्त अन्य कवियों में कुतुब वन दाऊद मंजन उस्मान आदि उल्लेखनीय हैं। इस शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का व्यापक प्रयोग किया है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास इस शाखा को काफी महत्वपूर्ण बताता है।
सगुण काव्यधारा
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में इस काव्य धारा की मान्यता है कि परमात्मा के सगुण रूप की उपासना करनी चाहिए शगुन काव्यधारा अभी कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा में विभाजित हो गई है।
कृष्ण भक्ति शाखा–हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में इस शाखा के अंदर कृष्ण भक्ति को प्रधानता दी गई है। इस शाखा में कृष्ण गोपी राधा ही आराध्य है अतः कृष्ण का भ्रम रूप में चित्रण किया गया है तथा इस शाखा के अंतर्गत नारी मुक्ति पर बल दिया गया है। इस शाखा के कुछ प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित है जैसे वल्लभ संप्रदाय, निंबार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय।
अष्टछाप–कृष्ण की उपासना के लिए अष्टछाप की स्थापना की गई जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास शामिल थे। सूरदास अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि थे।ब्रजभाषा का व्यापक प्रयोग में किया गया था।
रामभक्ति शाखा–हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से धर्म सदाचार एवं कर्तव्य परायणता का संदेश जनमानस तक पहुंचाने का कार्य रामभक्ति शाखा ने किया। राम के लोक नायक के रूप में उपासना लोकमंगल की सिद्धि सामान्य वाद पर बल इस शाखा की विशेषताएं रहीं। रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में रामानंद के प्रभाव से उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चली।
सर्व प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं जय श्री राम चरित्र मानस गीतावली विनय पत्रिका कवितावली आदि इसी शाखा की देन है। केशव की रामचंद्रिका भी इसी धारा का ग्रंथ है।
हमने कभी हमें अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास प्रिया दास प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम आदि थे। भाव अनुभव रस अलंकार सभी दृष्टि ओं में राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है।
भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता एकमात्र उद्देश्य था जिसके द्वारा समाज को ईश आराधना की ओर आकर्षित करना था। इस कॉल की प्रवृत्ति यह भी थी कि इस काल में गुरु की महिमा को स्वीकारा गया। तथा अहंकार के त्याग पर बल दिया गया। बहुजन हिताय की भावना पर भी जोर दिया गया। व्यष्टि के स्थान पर समस्त को महत्व दिया गया। आध्यात्मिक उन्नयन नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन ही अभीष्ट है।
भक्ति काल की गौण प्रवृतियां
वीर काव्य–श्रीधर का रणमल छंद, दुरसाजी आडा का विरुद्ध छतरी, दयाराम का राणा राशो। प्रबंधआत्मक चरित् काव्य–साधारू अग्रवाल–प्रद्युम्न चरित्र। शालिभद्र सूरी–पंच पांडव चरित् रास, आदि भक्ति काल की गौण प्रवृतियां में से प्रमुख हैं।
रीतिकाल (उत्तर मध्यकाल)
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई जिसका नाम रीतिकाल था तथा इसे उत्तर मध्य काल भी कहा गया। इस काल में भौतिकवादी विचारधारा को प्रमुखता प्रदान की गई। कविता साधन रहकर स्वयं शादी हो गई। रीतिकालीन कवियों का लक्ष्य काव्य शास्त्रीय अंगों का विवेचन तथा उदाहरण स्वरूप शृंगारिक काव्य की रचना करना था। आश्रय दाता का सहयोग पूर्ण वर्णन इसी काल में देखने को मिलता है अतः इस काल में तीन प्रकार की काव्य रचनाओं का वर्णन मिलता है।
- रीतिबद्ध रचना–नव रसों का सफल निरूपण आचार्य पद्माकर एवं सैयद गुलाम नबी रसली ने किया था।
| भूषण (वीर रस के कवि) | शिवराज भूषण |
| कवि जसवंत सिंह | भाषा भूषण |
| देव | भाव विलास |
| ग्वाल | रसरंग |
- रीति सिद्ध–इस श्रेणी में रीति ग्रंथों की रचना नहीं बल के काव्य सिद्धांतों के अनुसार ही रचना कि इस श्रेणी में बिहारी सेनापति विरेंद्र कृष्ण कभी नेवाज आदि उल्लेखनीय रचनाकार थे।
- रीतिमुक्त–आंतरिक अनुभूति भावावेश, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्ति, कल्पना की प्रचुरता आदि मुख्य विशेषताएं रीतिमुक्त की रही। प्रेम की पीर के कवि–घनानंद आलम बोधा ठाकुर आधे थे। मुक्तको की रचना नीति संबंधी रचनाएं–कवि वृंद, दीनदयाल, गिरि, गिरधरदास।
रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार से अंकित की गई हैं इन्हें याद करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकते हैं।
- रीत निरूपण
- श्रंगारिकता
- अलंकारिकता
- प्रारंभ में मंगलाचरण तथा अंत में आशीर्वचन जैसी भक्ति की प्रवृतियां काव्य में मिलती है।
- व्यक्तिक अनुभव के आधार पर नीतिपरक काव्य की रचना।
- प्रबंध एवं मुक्तक दोनों दृष्टि से समृद्ध बिहारी एवं धनानंद थे।
रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य
नीचे दी गई सारणी में रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य एवं उनके कवियों के नामों को अंकित किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं–
| कवि | ग्रंथ |
| चिंतामणि | रामायण, रामास्वमेघ, कृष्ण चरित्र |
| गोविंद सिंह | चंडी चरित्र |
| मंडल | जानकी जी का विवाह, पुरंदर माया |
| कुलपति मिश्र | द्रोण पर्व (संग्रामसार) |
| लाल कवि | छत्र प्रकाश |
| श्रीधर | जंगनामा |
| सुदन | सुजानचरित |
| पद्माकर | हिम्मतबहादुर विरुदावली |
| ग्वाल | हमीर हठ, विजय विनोद, गोपी पच्चीसी |
रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य
नीचे दी गई सारणी में रीतिकाल के कुछ प्रमुख मुक्तक काव्य एवं उनके कवियों का वर्णन किया गया है जो निम्न प्रकार से है–
| कवि | काव्य |
| चिंतामणि | कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्यप्रकाश, छंद विचार |
| मतिराम | रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी। |
| भूषण | शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, |
| बिहारी | सतसई |
| रस निधि | रतनहजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारहमासी, गीत संग्रह, अरिल्ल, हिंडोला, सतसई । |
| जसवंत सिंह | अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, |
| आलम | अलामकेलि |
| देव | भावविलास, भावानिविलास, कुशल विलास, प्रेमचन्द्रिका, जाति विलास, रास विलास, सूजान विनोद, प्रेमतरंग, देवचरित्र, काव्य, रसायन, देवशतक, सुखसागर तरंग , प्रेमदीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीतिशतक। |
| घनानंद | सुजनहित प्रबन्ध, कृपाकन्द निबंध, वियोग बेली, इश्क्लता, यमुनायश, प्रीतिपावस, पदावली, प्रकीर्णन छंद आदि। |
| रसलीन | अंगदर्पण, रस प्रबोध |
| सोमनाथ | रसपीयुषनिधि, शृंगारविलास, प्रेमपचीसी |
| भिखारी दास | काव्य निर्णय, श्रंगार निर्णय, रस सारांश, छन्दारनाव पिंगल, छंद प्रकाश। |
| दुलह | कविकुल कंठाभरण। |
| बोधा | विरह वारीश, इश्कनामा |
| पद्माकर | जगद्विनोद, पदमाभरण, गंगालहरी, प्रबोधपचासा, कलि पचीसी, प्रताप सिंह विरुदावली |
| बेनी बंदी जन | टिकेतराय प्रकाश, भड़ौवा संग्रह, रस विलाश |
| ग्वाल | यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिका नन्द, रसरंग, कृष्ण जू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधाष्टक, राधामाधव मिलन, कवि ह्रदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्ठक, षडऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, द्रगशतक |
| द्विज देव | श्रंगार लतिका, श्रंगार बत्तीसी, श्रंगार चालीसा, कविकल्पद्रुम। |
| जसवंत सिंह द्वितीय | श्रंगार शिरोमणि। |
आधुनिक काल
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बताता है कि रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल का आरंभ हुआ इस काल का आरंभ 18 सो 50 ईस्वी से अब तक माना जाता है इस काल के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं।
विभाजन
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में यह बताया गया है कि पुनर्जागरण काल यानी जिसे भारतेंदु युग कहां जाता है अट्ठारह सौ पचास से 1900 ईसवी तक तक चला
जागरण सुधार कल्याणी द्विवेदी युग उन्नीस सौ से 1918 ईस्वी तक छायावादी काल 1918 से 1938 ईस्वी तक और छायावादोत्तर काल 1938 से 1953 ईस्वी तक
भारतेंदु युग
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार भारतेंदु युग को कहा जाता है नवीन एवं प्राचीन का संधि योग भारतेंदु युग को ही कहा जाता है भारतेंदु युग नेगी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक दिए हैं। भारतेंदु के काव्य में भारतीय अतीत की गौरव गाथा तत्कालीन दुर्दशा पर छोड़ भरी भेजना तथा भक्ति के पद एवं श्रंगार एक छंद और नीति उपदेश तथा प्रकृति वर्णन आदि विद्यमान है।p भारतेंदु के अलावा इस युग में प्रताप नारायण मिश्र अंबिकादत्त व्यास राधा कृष्ण दास बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जगमोहन सिंह आदि उल्लेखनीय रचनाकार है।
जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग
द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1930 में संपादक बने अपने प्रयासों से उन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य का संपूर्ण विधान परिवर्तित कर दिया। इन्होंने खड़ी बोली का परिष्कार किया। साहित्य में जीवन जगत के सभी विषय शामिल हिंदी साहित्य का क्षेत्र व्यापक हुआ। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में इसी युग में भाषा छंद एवं अन्य साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति प्राप्त हुई।
मैथिलीशरण गुप्त की किसान तथा सियारामशरण गुप्त की अनाथ मानवतावादी दृष्टिकोण की कविताएं भी हमें इसी युग से प्राप्त हुई। इस युग के प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त को माना जाता है उनकी रचनाओं में से कुछ प्रमुख रचनाएं जिनके नाम निम्नलिखित हैं–
साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि
द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं
युग की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि यह इतिवृत्तआत्मकता एवं उपदेशआत्मकता और गद्यभाषादेने वाली काव्य शैली इस युग की प्रमुख विशेषताएं रही।
छायावाद काल
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में छायावाद काल सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक रहा इस काल में मुक्त छंद में अनुभूतियों को वाणी देने का प्रयास किया गया। दैनिक जीवन की विसंगतियों एवं विषमताओं से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति एवं अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए। प्रतीकात्मकता, अप्रस्तुत विधान, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता आदि छायावादी काव्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद की लघु यात्री महादेवी वर्मा रामकुमार वर्मा एवं माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है।
| कवि | रचनाएँ |
| जयशंकर प्रसाद | आँसूं , कामायनी, लहर |
| निराला | परिमल, गीतिका, अनामिका |
| पन्त (प्रकृति एवं सुकुमार कल्पना कवि) | ग्रंथि, पल्लव, गुंजन |
| महादेवी ( आधुनिक काल की मीरा ) | नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत |
छायावादी कविता के हास के कारण
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में विदेशी शासन के दमन चक्र से जन सामान्य की निरंतर बढ़ती पीड़ा इस पीड़ा ने कवियों को मनो लोग की दुनिया तथा कल्पना के प्रदेश से निकाल कर के यथार्थ की कठोर भूमि पर खड़ा कर दिया।
छायावादोत्तर काल
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में इस काल में जनता के दुख-दर्द को कविता का विषय बनाया गया। मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद का दर्शन अपनाया गया तथा मन के भीतर के यथार्थ को बाहर लाने के लिए सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण को उपयोगी समझा गया इसी को साहित्य में क्रमशः प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई।
प्रगतिवाद
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में मार्क्सवाद की अवधारणा पर आधारित रूसी साम्यवाद से प्रेरणा लेकर भारत में शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया। शिवमंगल सिंह सुमन, डॉ रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन, रंगे राघव केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख कवि थे। पंत, निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि प्रगतिवादी रचनाएं लिखने लगे। शिवमंगल सिंह सुमन नहीं लिखा लाल झंडा और मास्को अभी दूर है। वही त्रिलोचन ने लिखा मिट्टी की बारात एवं धरती की सोंधी गंध।
प्रयोगवाद
इसमें फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित व्यक्तिवाद की परिणति घोर अहमवादी तथा स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, एवं असंतुलित मनोवृति के रूप में हुआ है। यह काव्यधारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। वर्ष 1943 में आगे द्वारा तार सप्तक प्रकाशित हुआ इसमें अज्ञेय मुक्तिबोध गिरिजाकुमार माथुर प्रभाकर मच्वे नेमी चंद्र जैन भारत भूषण अग्रवाल एवं रामविलास शर्मा शामिल थे।
दूसरा सप्तक – वर्ष 1951 में प्रकाशित हुआ। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती शामिल थे।
तीसरा सप्तक – वर्ष 1959 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण साही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शामिल थे।
चौथा सप्तक – वर्ष 1979 में प्रकाशित हुआ। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर, आचार्य सुमन राज, श्री राम वर्मा एवं राजेंद्र किशोर शामिल थे। व्यक्तित्व वाद की चरम परिणति, अहंवाद, परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार, जीवन आदर्शों के प्रति अनास्था, सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्य के कारण कुंठा एवं वेदना से ग्रस्त अदि प्रवृतियां प्रमुख थी।
नई कविता
वर्ष 1954 ईस्वी से नई कविताओं का प्रारंभ हुआ जो अब तक चली आ रही है वर्ष 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसमें एक ऐसे मानव की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया जो स्वस्थ सामाजिक जीवन दर्शन को तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक संप्रक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा सपाट बयानी पर जोर दिया गया है।
अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिराज कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा ,केदारनाथ सिंह , कैलाश बाजपेई आदि इस आंदोलन के उल्लेखनीय कवि हैं।
नवगीत
वर्ष 1957 में इलाहाबाद के साहित्य सम्मेलन की कविता गोष्ठी में वीरेंद्र मिश्र द्वारा नवगीत की स्पष्ट घोषणा की गई। इसमें छायावाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रवृत्तियों का मिश्रण है।
डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, गोपाल प्रसाद सक्सेना, गोपालदास नीरज, रामनाथ अवस्थी, रामावतार त्यागी के अतिरिक्त रामानंद दोषी, बालस्वरूप राही, डॉ रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, उमाकांत मालवीय, ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेंद्र शर्मा इंद्र, चंद्रसेन विराट, दिनकर सोनवलकर, सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, रमेश रंजन, सारस्वत मोहन मनीषी, सुरेश वात्सायन, मुकुट बिहारी सरोज, श्रीकृष्ण तिवारी माहेश्वर तिवारी आज उल्लेखनीय गीतकार है।
साठोत्तरी कविता
इस काव्य आंदोलन में निर्मम वास्तविकता की क्रूर व्यंजना है। भयानक परिवेश से उपजी चीख है। मोह-भंग आक्रोश अस्वीकार तनाव और विद्रोह की कविताएं हैं इसमें जिजीविषा का गहरा रंग है। धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, बलदेव वंशी, जगदीश चतुर्वेदी, रामदरश मिश्र, गोरख पांडे, अरुण कमल, कुमारेंद्र, सुरेश तिवारी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, कुमार विकल आज इस आंदोलन के उल्लेखनीय कवि हैं।
नया दोहा
समसामयिक जीवन की वास्तविकता का प्रकटीकरण नया दोहा में ही मिला इस के प्रवर्तक कवि पंडित देवेंद्र शर्मा थे जिन की एक रचना आंखों खिले पलाश वर्ष 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई इसमें 1000 का संकलन किया गया था। इसमें प्रमुख कवि देवेंद्र शर्मा, पाल भसीन, विजय प्रकाश दीक्षित, भारतेंदु मिश्र, दिवाकर आदित्य शर्मा और बाबू राम शुक्ला उल्लेखनीय है
हिंदी गजल
दुष्यंत कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका समकालीन जीवन की वास्तविकता से पाठक को परिचित कराती है दुष्यंत के अतिरिक्त कुंवर बेचैन एवं अदम गोंडवी उल्लेखनीय है इसके अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, राम अवतार त्यागी इनके अलावा वशिष्ठ अनूप, शलभ श्री राम सिंह, शिव ओम अंबर, मधुर नजमी, कमल किशोर श्रमिक, अवध नारायण मुद्गल, चंद्रसेन विराट, उर्मिलेश आदि उल्लेखनीय रचनाकार है।
हिन्दी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ
भारतेन्दु युग
| पत्रिका का नाम | सम्पादक का नाम | प्रकाशन स्थान |
| कवि-वचन सुधा | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | काशी |
| हरिश्चन्द्र मैग्जीन | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | काशी |
| हिन्दी प्रदीप | बालकृष्ण भटट | इलाहाबाद |
| आनन्द कादम्बिनी | बद्रीनारयण चौधरी प्रेमघन | मिर्जापुर |
| ब्राह्मण | प्रतापनारायण मिश्र | कानपुर |
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास
द्विवेदी युग
| सरस्वती | आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | इलाहाबाद |
| सुदर्शन | देवकीनन्दन खत्री /माधवप्रसाद मिश्र | काशी |
| समालोचक | चन्द्रधर शर्मा गुलेरी | जयपुर |
| इन्दु | अम्बिकाप्रसाद गुप्त | काशी |
| मर्यादा | कृष्णकांत मालवीय | प्रयाग |
| प्रताप | गणेश शंकर विद्यार्थी | कानपुर |
| प्रभा | बालकृष्ण शर्मा नवीन | खण्डवा |
| चाँद | रामरख सहगल/चण्डीप्रसाद ह्रदयेश | प्रयाग |
| माधुरी | दुलारेलाल भार्गव | लखनऊ |
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास
छायावादी युग
| हंस | प्रेमचन्द्र | काशी |
| आदर्श/मौजी | शिवपूजन सहाय | कलकत्ता |
| सरोज | नवजादिक लाल श्रीवास्तव | कलकत्ता |
| साहित्य-सन्देश | गुलाबराय | आगरा |
| कर्मवीर | माखनलाल चतुर्वेदी | जबलपुर |
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास
छायावादोत्तर युग
| कादम्बिनी | राजेन्द्र अवस्थी | दिल्ली |
| धर्मयुग | धर्मवीर भारती / गणेश मन्त्री | बम्बई |
| सारिका | कमलेश्वर/अवधनारायण मुदगल | दिल्ली |
| हंस | राजेन्द्र यादव | दिल्ली |
| गंगा | कमलेश्वर | दिल्ली |
हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास
| अन्य प्रमुख पत्रिकाएँ | सम्पादक |
| मर्यादा टुडे | डॉ सम्पूर्णानन्द |
| तरुण भारती | रामवृक्ष बेनीपुरी |
| नया जीवन | कनैयालाल मिश्र प्रभाकर |
| वसुधा | हरिशंकर परसाई |
यह भी पढ़े – आन का मान नाटक का सारांश 2022-2023